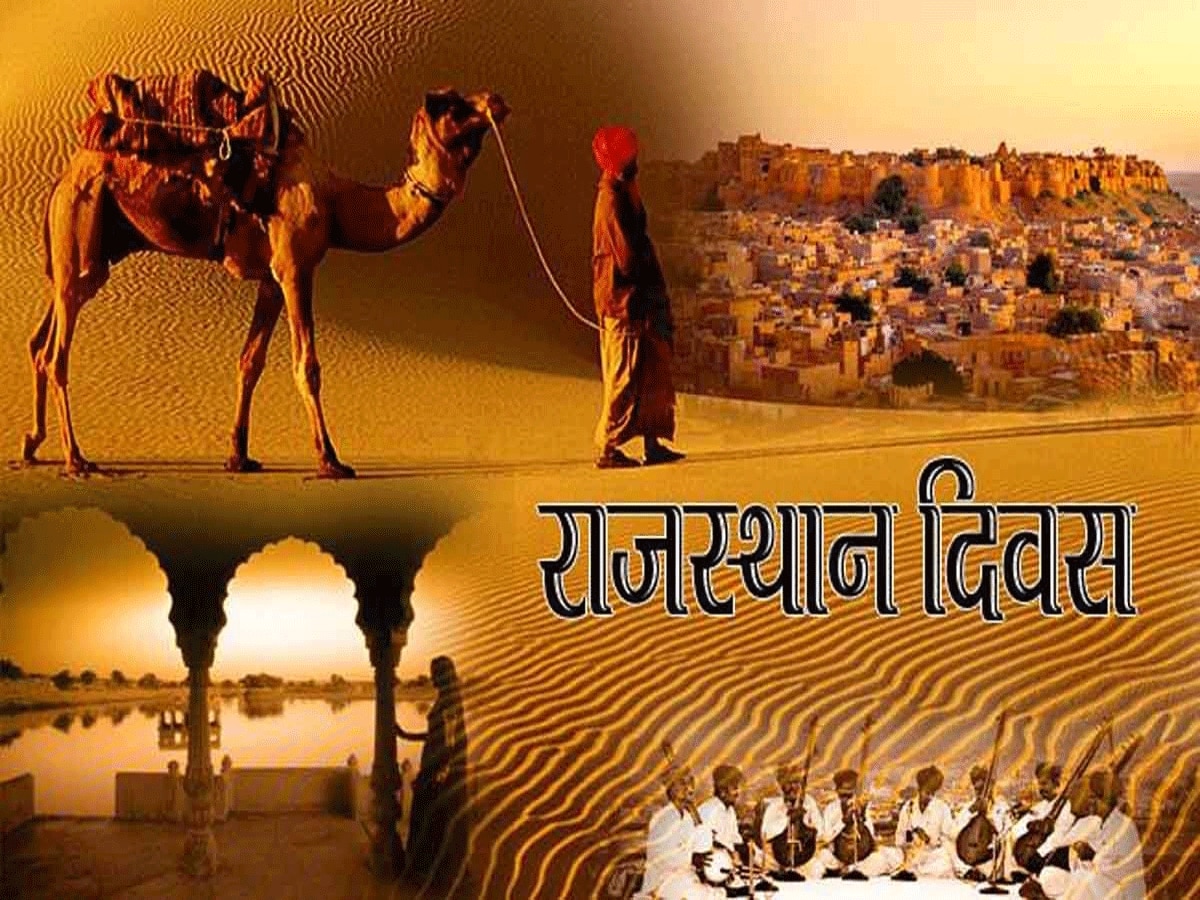भारत और IPEF : भारत ने IPEF में शामिल होने का फ़ैसला क्यों किया? जानिए भारत के लिए चुनौती तथा जिम्मेदारियाँ
India and IPEF: भारत और अमेरिकी नीत इस गठबंधन में ऐसे कई मसले हैं जिन्हें लेकर भारत और अमेरिका के नज़रिए में व्यापक फ़र्क़ है,जिसे कई मंचों पर बेहद संजीदगी के साथ महसूस किया गया है,जैसे भारत के लिए ऊंचे मानक हमेशा ही एक परेशानी की बात रहे हैं। शायद इसी वजह से भारत ने कभी भी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) को गंभीरता से नहीं लिया.

यहां यह गौर करना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत ने हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे का सदस्य बनने के लिए हिचकते हुए क़दम उठाए हैं बीते 21 मई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक सवाल के उत्तर में कहा कि यह एक अमेरिकी पहल है और भारत इस पर "विचार'' कर रहा है लेकिन, 23 मई को जब इसकी औपचारिक घोषणा हुई ,तो वहां मौजूद क्वॉड के तीन नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे।
भारत और अमेरिकी नीत इस गठबंधन में ऐसे कई मसले हैं जिन्हें लेकर भारत और अमेरिका के नज़रिए में व्यापक फ़र्क़ है,जिसे कई मंचों पर बेहद संजीदगी के साथ महसूस किया गया है,जैसे भारत के लिए ऊंचे मानक हमेशा ही एक परेशानी की बात रहे हैं। शायद इसी वजह से भारत ने कभी भी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) को गंभीरता से नहीं लिया.
डिजिटल प्रशासन के नियम भी शायद भारत की वर्तमान स्थिति के लिहाज़ से बेहद विरोधाभासी हैं,डेटा के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह, डेटा को स्थानीय स्तर पर,ख़ास तौर से वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संरक्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से विकसित किए जाने वाले डिजिटल उत्पादों पर सीमा शुल्क जैसे मुद्दों पर भारत और अमेरिका के नज़रिए में ख़ासे मतभेद मौजूद हैं।
अमेरिका के संघीय और राज्यों के क़ानून अक्सर उन नियमों के विरोधाभासी होते हैं जिन्हें भारत तरज़ीह देता है. यही बात भारत और अन्य विकसित देशों के बीच कई नीतिगत मतभेद हैं, विशेषकर श्रम मानकों, श्रमिक सुधार,सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए सीमा के आर-पार की सब्सिडी और ऐसी संस्थाओं की भूमिका को लेकर दोनों के बीच नज़रिए में व्यापक मतभेद और असन्तुलन व्याप्त है। यहां गौर करना होगा कि नवगठित IPEF में विकसित और विकासशील, दोनों ही देश शामिल हैं और ऐसे में इस तरह के विरोधाभासी मतभेद बेहद आसानी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं.
अगर IPEF के सदस्य संरचना पर एक सरसरी नजर डाली जाए तो हम पाते हैं कि उसने अपनी शुरुआती दौर में 13 देशों को अपने साथ लाने में सफल रहा है,जिसमे "एशियन टाइगर" कहे जाने वाले "आसियान10'' के सात देशों शामिल है जो इस आर्थिक ढांचे को लेकर सलाह मशविरों में शामिल होने पर सहमति जताई है।
इसके अतिरिक्त क्वॉड के चार देश- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का शामिल होना नैसर्गिक था। इनके अलावा हम फाइव ऑय समूह से न्यूज़ीलैंड और हिन्द प्रशांत क्षेत्र में जबरदस्त आर्थिक दमखम वाला देश दक्षिण कोरिया को भी इस आर्थिक ढांचे का हिस्सा बनते देख रहे है।
यहां एक बात और भी गौर करने वाली है आईपीईएफ के ये सभी 13 देश ईस्ट एशिया समिट के सदस्य हैं और अगर भारत और अमेरिका को छोड़ दें तो बाक़ी के 11 देश, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) का भी अभिन्न हिस्सा हैं।
ऐसे में सवाल उठना बेहद लाजिमी है कि आख़िर भारत ने IPEF में शामिल होने का फ़ैसला क्यों किया?
विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे ज़्यादातर अघोषित सामरिक कारण हैं, जो संभवतः 2012 में भारत के व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी (RCEP) में शामिल होने की वजह बने थे।
अगर क्वॉड शिखर सम्मेलन के दौरान अगर भारत IPEF का सदस्य नहीं बनता,तो वो उस मौक़े पर भारत ख़ुद को पूरी तरह से अलग-थलग होने की पूरी गुंजाइश थी,चूंकि अमेरिकी नीत इस पहल को हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक समर्थन मिल रहा है. ऐसे में भारत के लिए हाशिए पर पड़े रहना किसी भी रूप में फ़ायदेमंद नहीं होता।
मौजूदा दौर में सामरिक,रणनीतिक, आर्थिक और आसूचना की दृष्टिकोण से फिलहाल क्वाड देश पूरे हिन्द प्रशांत क्षेत्र की सिक्यूरिटी आर्किटेक्कर को संतुलित करने में सफल होते दिख रहे है। हालांकि यह एक बेहद रोचक तथ्य है कि ,ऐसा पहली बार हुआ जा,जब भारत, हिंद प्रशांत क्षेत्र की किसी बहुपक्षीय आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बना है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की इस पहल से भारतीय राजनय का सशक्त और सकारात्मक नज़रिया सामने आया है। भारत के लिए यह बेहद अहम चुनौती होगी कि वह इन तमाम देशों के साथ अपने तमाम "द्वंदात्मक और भेदभावपूर्ण नियमों" में "अपने हितों को अक्षुण्ण रखे" और इस आर्थिक ढांचे से भारत के लिए अधिकतम लाभ निकाल सके।
वहीं,अमेरिका, IPEF को एक ऐसे भरोसेमंद ढांचे के तौर पर देखना चाहता है , जो उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके खोये हुए आर्थिक संबंधों में नई जान डाल सके, अमेरिका को IPEF से उम्मीदें तो जगती है,साथ ही उसके लिए एक चनौती है कि अगर इसके ज़रिए अमेरिका अपने आर्थिक और सामरिक हितों को साधना चाहता है तो इसके लिए IPEF को नियम आधारित और पारदर्शी तरीके से उसे आगे बढ़ाना होगा,उसे अपने अपने बाज़ार की पहुंच समान रूप से भारत सहित अन्य सदस्य देशों को देनी ही होगी जिससे IPEF को सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला भरोसेमंद विकल्प बन सकेगा।
चूंकि अमेरिका वैश्विक महाशक्ति है इसलिये उसे,"अंकल सैम"की भूमिका से बाहर निकलते हुए और अपने कद अनुरूप व्यवहार करते हुए उसे अन्य क्षेत्रीय पहलों को मज़बूत बनाने में सहयोगी भूमिका निभानी होगी, जिससे कि अमेरिका के दोस्त और साझीदार देश IPEF को इस क्षेत्र में उसे एक उपयोगी और विश्वसनीय वादे को पूरा करने वाला देश और "मित्र राष्ट्र" के तौर पर देख सकें।
आईपीईएफ के आगाज वाले पूरे सत्र में एक बार भी चीन की चर्चा नहीं कि गयी,जो राजनायिक दृष्टिकोण से बेहद परिक्व फैसला था, दरअसल चीन IPEF को अमेरिका की उसी कोशिश का एक हिस्सा मानता है, जिसकी मदद से अमेरिका ख़ुद को चीन की अर्थव्यवस्था से अलग कर सके।
इससे पहले क्वाड गठबंधन की खिल्ली उड़ाने वाला चीन इस समझौते को आसियान की एकता को कमज़ोर करने की भी एक पहल के तौर पर देखता है, जिससे अमेरिका,आसियान देशों को अपनी हिंद प्रशांत रणनीति का हिस्सा बना सके।
चीन का मानना है कि IPEF, आसियान देशों को उसकी अर्थव्यवस्था से अलग करने में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीन और आसियान देशों के बीच गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं।
आईपीईएफ में भारत का क्या होगा योगदान?
आईपीईएफ में भारत की भूमिका की बात करें तो 'स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु प्राथमिकताओं, महामारी को लेकर तेज प्रतिक्रिया,आपूर्ति श्रृंखला विविधता और लचीलापन, उभरती टेक्नोलॉजी, निवेश स्क्रीनिंग' के विकास के लिए बेहद 'महत्वपूर्ण' है।
अमेरिका का मानना है कि, भारत इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ सकारात्मक आर्थिक जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। अमेरिका इस क्षेत्र में भारत के प्रभावी प्रभुत्व से बेखबर नहीं है इसलिए वह मानता है कि, वर्तमान वैश्विक परिवेश में भारत और अधिक विविध,समावेशी और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में एक अभिन्न भूमिका निभाएगा।
इसी कड़ी में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो का यह बयान बेहद प्रासंगिक हो जाता है जिसमे उन्होंने व्यापारिक प्लेटफॉर्म को लांच करने के बाद कहा कि, 'यह (आईपीईएफ) इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक जुड़ाव है। और इसका शुभारंभ, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी आर्थिक नेतृत्व को बहाल करने और इंडो-पैसिफिक देशों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चीन का विकल्प बनने का एक प्लेटफॉर्म बनाना है'। यानि, आने वाले वक्त में इस प्लेटफॉर्म से इंडो-पैसिफिक देशों के सामने आयात-निर्यात का एक अलग विकल्प खुल जाएगा।
आईपीईएफ से भारत को संभावित लाभ ?
भारत और चीन के बीच की व्यापारिक भागीदारी 125 अरब डॉलर को पार कर गई है, लेकिन भारत- चीन के बीच सीमा पर पिछले दो वर्षो से जारी व्यापक रूप से तना तनी के वावजूद भारत के साथ व्यापार असन्तुलन व्याप्त है। इस साल चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 88 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते है कि यह आंकड़ा भारत के रक्षा बजट को पार कर चुका है।
भारत के तमाम अनुरोधों के बाद भी चीन भारत से तयशुदा सामनों का आयात नहीं करता है जिससे व्यापारिक असन्तुलन बढ़ता ही जा रही है,लिहाजा,आईपीईएफ,भारत के लिए एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है ,अगर, इसके प्रावधानों को सही से लागू किया जाए और अमेरिकी बाजार उसे प्राप्त हो सके। पीएम मोदी ने ट्रेड पार्टनरशिप के लॉन्च इवेंट में कहा कि, 'आईपीईएफ हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक विकास के इंजन में बदलने की हमारी सामूहिक इच्छा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा और रचनात्मक समाधान खोजने का भी आह्वान भी किया।
साथ ही उन्होंने कहा कि,'आईपीईएफ भारत-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है'।
जाहिर है,भारतीय सामानों/मालों के लिए ही ना सिर्फ व्यापक बाजार मिलेंगे बल्कि भारत इन देशों से ऐसे सामान भी आसानी से आयात कर सकता है, जिसके लिए भारत को चीन पर निर्भर रहना पड़ता है।
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ )
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस रणनीति का हिस्सा है,जिसमें वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग होने के फैसले को बदलते हुए इस क्षेत्र में अमेरिकी नीत हिन्द प्रशांत आर्थिक फोरम(आईपीईएफ) के जरिये नए तरह के व्यापारिक समझौते को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आईपीईएफ के जरिए एक बार फिर से पूरे हिन्द प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की नई भूमिका, क्षेत्र में विभिन्न मसलों पर बढ़ती अमेरिकी हिस्सेदारी और प्रभावी विश्वसनीयता को बढ़ाना चाहते हैं।
इस संगठन में अमेरिका के अलावा 12 और देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया,जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया,न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं,यानि कुल 13 देशों का ये गठबंधन दुनिया की कुल जीडीपी का 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं।
सबसे खास बात यह है,कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर इस संगठन के सभी साझेदार एशिया महाद्वीप के हैं और उससे भी सबसे बड़ी बात ये हैं, कि इनमें से ज्यादातर देश चीन के पड़ोसी हैं और चीन के साथ इनके तमाम पहलुओं वाले रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए इस व्यापारिक मंच को बनाने का मकसद ही हिन्द प्रशांत क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ चीन के आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करना है।
वे आईपीईएफ के सदस्य देशों के बीच अधिक से अधिक आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित करने पर जोर देने की जोर आजमाइश करने में किसी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते है। इस सबका उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जिसमें सदस्य देश अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बातचीत के लिए साथ आ सके।
यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के इनसाइट पेपर के एक अध्ययन के अनुसार आईपीईएफ कोई परंपरागत व्यापार समझौता नहीं है,बल्कि इसमें कई अलग-अलग मॉड्यूल शामिल होंगे, जिनमें "फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड", "सप्लाई चेन रेजिलियंस', "इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डिकार्बनाइजेशन " के साथ साथ "कर और भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई" शामिल है। इसमें शामिल होने वाले देशों को एक मॉड्यूल के सभी अवयवों में शामिल होना होगा,लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उन्हें इस समझौते के सभी मॉड्यूल में शामिल होने की जरूरत है।
इस समझौते के प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड की अगुवाई यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव(यूएसटी आर) करेंगे, जिसमें डिजिटल, श्रम और पर्यावरण और परिस्थितिकी से संबंधित मुद्दे होंगे। सम्भव है कि इनमें से कुछ बाध्यकारी होंगे। वहीं,आईपीईएफ में टैरिफ बैरियर कम करने जैसे मुद्दे नहीं होंगे।
इसलिए विशेषज्ञ इस समझौते को यह एक तरह का "एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट''की संज्ञा दे रहे हैं,जिसके लिए किसी देश को इसमें शामिल होने के लिए अपने संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। वहीं, व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए संसद के अनुसमर्थन आवश्यक है।
चीन फैक्टर
आईईपीएफ के आगाज के पूरे सत्र में खुले तौर पर किसी सदस्य देशों ने चीन का एक दफे कहीं पर भी जिक्र नहीं किया,यह एक बेहद परिपक्व राजनय को दर्शाती है।
हिन्द प्रशांत क्षेत्र में चीन की विभिन्न प्रकार की सक्रियता किसी से छिपी नहीं है,और बदलते वैश्विक घटनाक्रम में इस समझौते को बेहद संजीदगी के साथ महसूस की जा रही थी ।
यहां यह बेहद आवश्यक था कि आईपीईएफ(IPEF) को चीन से दूर एक अलग आर्थिक धुरी के रूप में भी देखा जाय । दरअसल एशिया में दो प्रमुख कारोबारी समूह सीपीटीपीपी (CPTPP) और आरसीईपी (RECP) पहले से मौजूद है हैं। जहां तक चीन की बात है तो वह ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी सीपीटीपीपी (CPTPP) की सदस्यता की आकांक्षा रखता है, वहीं वह रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RECP) का सदस्य है।
मौजूद दौर में अमेरिका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप(TPP) से अलग हो चुका है और वह RECP का वह सदस्य नहीं है। अमेरिका की तरह भारत भी इन दोनों कारोबारी समूह का सदस्य नहीं है, ऐसे में अमेरिका की कोशिश यह है कि वह IPEF के जरिए इस क्षेत्र में न केवल चीन के दबदबे को रोके बल्कि इस क्षेत्र में फिर से अपनी पुरानी विश्वसनीयता को कायम करे,और वैश्विक प्रभामण्डल पर भारत के बिना यह कार्य मृगतृष्णा के समान है।
अमेरिका को इस भगीरथ कार्य में भारत उसका अहम साझेदार बनाना आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के सिद्धान्तों के हिसाब से बेहद मुफीद है और जिसका मकसद इंडो-पैसिफिक यानि भारत-प्रशांत क्षेत्र में, जहां चीन का प्रभाव बन रहा है, वहां व्यापारिक भागीदारी को चीन के प्रभाव से मुक्त होकर आगे बढ़ाना है।